Table of Contents
वह पल जब ज़िंदगी रुक जाती है
आजकल हम फिल्मों और टीवी शो में देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स, सीपीआर देकर किसी की जान बचाते हैं। हमें भी पता है कि आपात स्थिति में क्या करना चाहिए।
लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए: आप अपने परिवार के साथ हैं और अचानक एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, उसकी साँसें थम जाती हैं और दिल धड़कना बंद कर देता है।

कुछ मिनट पहले जो इंसान आपसे बात कर रहा था, वह अब शांत हो चुका है। 1950 के दशक तक, ऐसे में हर कोई असहाय महसूस करता था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उम्मीद नहीं।
यह कहानी है उसी पल में उम्मीद जगाने वाले एक सरल और शक्तिशाली तरीके की, जिसे हम सब सीपीआर CPR के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है।
प्राचीन प्रयास: जब इंसान ज़िंदगी वापस लाने की कोशिश करता था
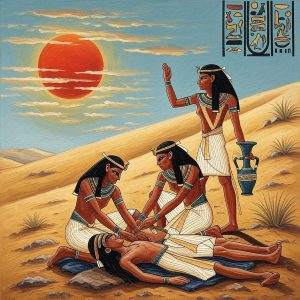
सीपीआर का विचार 3,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मिस्र के प्राचीन एबर्स पेपाइरस (Ebers Papyrus) में यह दर्ज है कि कैसे डूबे हुए लोगों को गर्म रेत में लिटाकर होश में लाने की कोशिश की जाती थी।
लगभग 800 ईसा पूर्व, बाइबिल में यह भी लिखा है कि पैगंबर एलिजा (Elisha) ने एक बच्चे के मुँह में साँस देकर उसे फिर से ज़िंदा किया। यह कृत्रिम साँस (artificial ventilation) का सबसे शुरुआती लिखित रिकॉर्ड है।
16वीं सदी तक, स्विस चिकित्सक पैरासेल्सस (Paracelsus) ने फेफड़ों में हवा भरने के लिए धौंकनी (bellows) का इस्तेमाल किया।
फिर 1767 में, डच बचावकर्मियों ने दुनिया का पहला संगठित पुनर्जीवन समाज (resuscitation society) बनाया। ये लोग छाती पर दबाव देने और मुँह से मुँह में साँस देने के तरीकों की वकालत करते थे।
आधुनिक सीपीआर से पहले का युग: विज्ञान की शुरुआत (19वीं सदी)
19वीं सदी में, शरीर विज्ञान की समझ बढ़ने लगी। इस दौर में एक महत्वपूर्ण खोज हुई, जिसने सीपीआर की नींव रखी।
1891 में, जर्मन डॉक्टर फ्रेडरिक मास (Friedrich Maass) ने पहली बार इंसान पर छाती पर दबाव देने का सफल प्रयोग किया।
उन्होंने लगातार 45 मिनट तक एक किशोर पर दबाव डालकर उसे होश में लाया। हालाँकि, इस तकनीक को तब ज़्यादा मान्यता नहीं मिली।
डॉक्टर तब दिल को पुनर्जीवित करने के लिए छाती खोलकर दिल को हाथ से दबाने के तरीकों को ज़्यादा पसंद करते थे, जो सिर्फ अस्पतालों में ही संभव था।
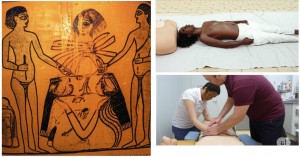
आधुनिक सीपीआर का जन्म (1950-1960)
यही वह समय था जब सीपीआर को एक वैज्ञानिक आधार मिला।
1954 में, डॉ. पीटर सफार ने यह वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया कि मुँह से मुँह में साँस देना, किसी भी अन्य तरीके से बेहतर है।
उन्होंने “A-B-C” (Airway-Breathing-Circulation) प्रोटोकॉल की नींव रखी।
फिर 1960 में, जॉन्स हॉपकिन्स के शोधकर्ताओं, जिनका नेतृत्व डॉ. विलियम कौवेनहोवन (Dr. William Kouwenhoven) कर रहे थे, ने एक बड़ी खोज की।
उन्होंने पाया कि दिल का दौरा पड़ने पर छाती को खोले बिना भी उस पर दबाव डालकर खून का बहाव बनाए रखा जा सकता है।
उनके इस शोध ने डॉ. सफार की साँस देने की तकनीक को छाती पर दबाव देने के साथ मिला दिया। इसी तरह, आधुनिक सीपीआर का जन्म हुआ, और इसका प्रकाशन JAMA (Journal of the American Medical Association) में हुआ।
साँस और धड़कन का तालमेल: सीपीआर का विज्ञान
ऑक्सीजन की आपूर्ति: दिमाग को बचाने का पहला कदम
जब कोई व्यक्ति साँस लेना बंद कर देता है, तो उसके फेफड़ों में जो थोड़ी बहुत हवा और ऑक्सीजन होती है, वह कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है।
हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग, दिमाग, ऑक्सीजन के बिना सबसे जल्दी क्षतिग्रस्त (damaged) हो जाता है। अगर तीन से पाँच मिनट तक दिमाग को ऑक्सीजन न मिले तो उसकी कोशिकाएँ हमेशा के लिए मर सकती हैं।
इसीलिए, डॉ. सफार ने यह पाया कि मुँह से मुँह में साँस देना (mouth-to-mouth resuscitation) जीवन बचाने का सबसे पहला कदम है।
यह बंद हो चुकी साँसों के बीच दिमाग और बाकी अंगों को जीवित रखने के लिए एक पुल (bridge) की तरह काम करता है। यह हर साँस उस व्यक्ति को पेशेवर मदद मिलने तक ज़िंदा रखने की एक कोशिश है।
रक्त संचार को बनाए रखना: दिल को बाहर से धड़काना
जब दिल धड़कना बंद कर देता है, तो खून का संचार भी रुक जाता है। खून के ज़रिए ही ऑक्सीजन दिमाग तक पहुँचती है।
इस स्थिति में, छाती पर दबाव देना (chest compressions) एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है।यह दबाव दिल को बाहर से धड़काने का काम करता है।
जब आप छाती के बीच में जोर से दबाव देते हैं, तो यह सीधे दिल पर दबाव डालता है, जिससे खून शरीर से बाहर निकलता है।
और जब आप दबाव हटाते हैं, तो दिल वापस खून से भर जाता है। इस लयबद्ध (rhythmic) क्रिया से, खून लगातार दिमाग तक पहुँचता रहता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिल के फिर से काम करना शुरू करने तक या पेशेवर मदद पहुँचने तक शरीर को जीवित रखती है।
व्यापक प्रचार और नई तकनीकें (1970 से 21वीं सदी तक)

सीपीआर की खोज के बाद इसे आम लोगों तक पहुँचाने का काम शुरू हुआ। 1972 में, सिएटल में “मेडिक 2” (Medic 2) नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसने 1,00,000 से ज़्यादा आम नागरिकों को सीपीआर सिखाया।
इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया कि सार्वजनिक सीपीआर प्रशिक्षण जीवन बचा सकता है।
एईडी (AED): 1980 के दशक में, पोर्टेबल एईडी (AED) का आविष्कार हुआ। ये छोटे उपकरण थे जो खुद-ब-खुद दिल की धड़कन का विश्लेषण करके बिजली का झटका दे सकते थे।
हैंड्स-ओनली सीपीआर”: 2008 में, आम लोगों के लिए “हैंड्स-ओनली सीपीआर” का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सिर्फ छाती पर दबाव देने की ज़रूरत होती थी।
आज और भविष्य
आज, सीपीआर की तकनीक और भी उन्नत हो चुकी है। अब एआई-गाइडेड डिवाइस और ड्रोन से एईडी पहुँचाने जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है।
सीपीआर का यह सफर, प्राचीन मिस्र की रेत से शुरू होकर, आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक पहुँच गया है, और यह लगातार विकास कर रहा है।
aur unsuni kahaniyaan
इंजेक्शन का अविष्कार: जिस सुई ने बदल दी दर्द की दुनिया
Inhaler की कहानी: जब एक पिता ने अपनी बेटी के लिए उम्मीद की साँस ढूंढी
टाँके लगाने की डरावनी, पर कमाल की दास्तान


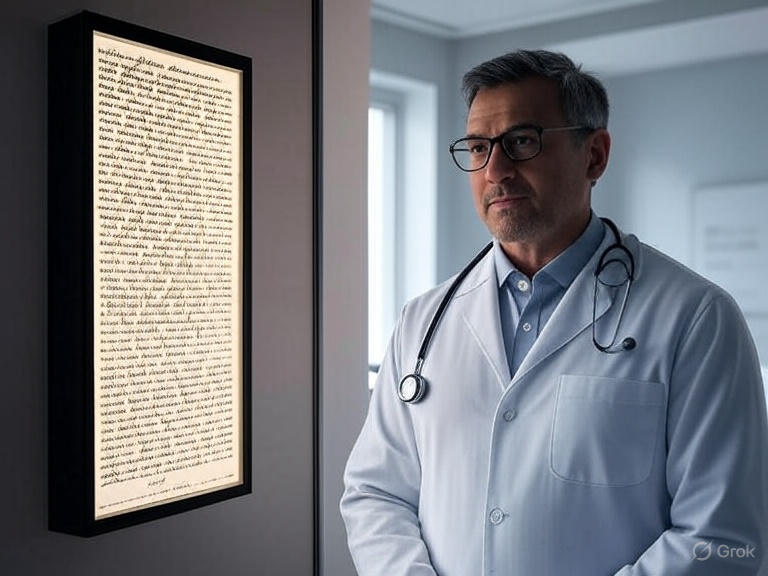
[…] CPR STORY:मौत और ज़िंदगी के बीच का फासला […]
[…] CPR STORY:मौत और ज़िंदगी के बीच का फासला […]